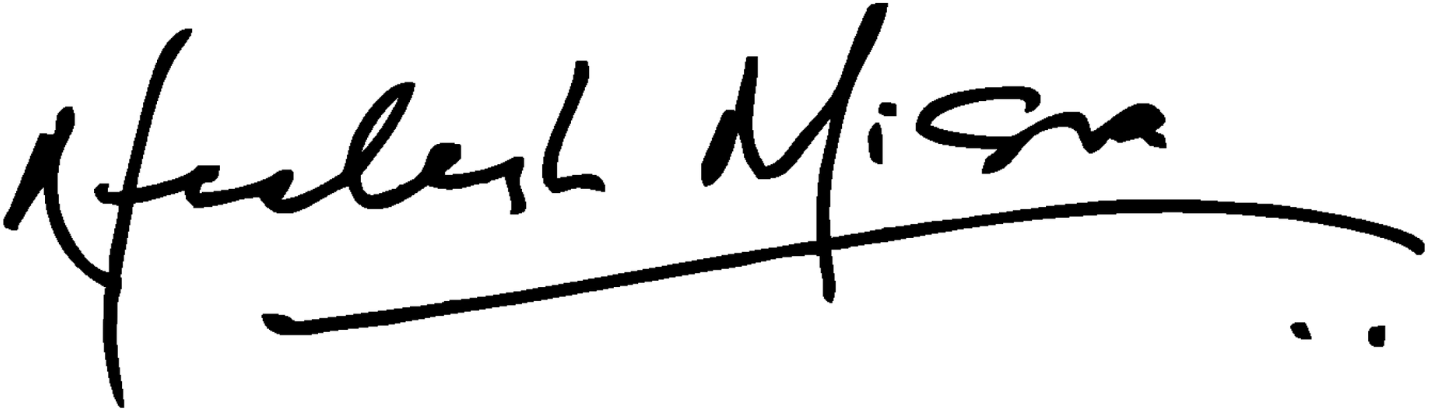गर्मियों की छुट्टियों का पहला महीना यानी हम सबका केरला (Kerala) ट्रिप ! केरला के एक छोटे से गाँव आइरूर में मेरा ददिहाल था। ज़िला पट्टनमथिट्टा और सड़क कांजीटूकेरा … हो गई ना जीभ गोल? बस यही वजह थी कि बचपन में मेरा मन भी गाँव याने केरला () जाने के नाम से घबराने लगता था। मध्यप्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्य में पैदा होने और पलने बढ़ने के कारण मलयालम भाषा मेरे लिए अनजानी ही रही और एक महीने लगातार वहां रहना यानी कि हर पल एक धुकधुकी कि कब कौन कुछ कह जाए और मैं बंगले झाँकती रह जाऊँ। वहाँ रहना याने लोगों से बात करते हुए हिचकिचाना…
हालांकि एक महीने रह कर थोड़ा बहुत सीख भी जाया करती लेकिन वो अगली ट्रिप तक दिमाग से फिर सफाचट हो जाता था और फिर वही हिचक तारी हो जाती। पर उम्र के साथ थोड़ा सा समझदार हुई यानी कि भाषा की समझ तो नहीं पर भावनाओं की समझ बढ़ी तब वहां जाना मन को ऐसा सुख देने लगा, जो किसी भी बच्चे को उसके दादा-दादी के घर में मिलता है, फिर ये तो केरला था, भगवान् का अपना देश …गॉड्स ओन कंट्री।
केरला (Kerala) में मेरे में दादा का घर एक ऊंची पहाड़ी पर बना था, पहाड़ी याने मल्लई। नारियल के ऊंचे और कटहल के घने घने पेड़ों के बीच आड़े टेड़े काले पत्थरों की सीढ़ियों से दौड़ते हुए, पेड़ों के तने से बने छोटे छोटे पुल पार करते हम एक सांस में ऊपर पहुंच जाते थे। इस मेहनत का इनाम मिलता था नारियल का मीठा-ठंडा पानी और कई तरह के केले, कोई एक हाथ बराबर तो कोई हथेली के जितना छोटा। ये फल इस प्रदेश की ख़ासियत है और रोज़ के खाने में शामिल है। बल्कि कई नाश्तों में पके केले का इस्तेमाल होता है। हम्म… लिखते हुए वो नारियल और केले की मिली जुली खुशबू याद आई। यहां एक भी व्यंजन ऐसा नहीं, जो नारियल के बिना बनता हो। मंदिरों में प्रसाद के तौर पर मिलता है नारियल का पानी और गुड़, पोहा मिला नारियल भी।
खाने पीने, पेड़ पहाड़, नदी नाले के अलावा जो चित्र मेरी आँखों में अब तक ताज़ा है वो है दादाजी का।
अपने दादाजी को मैंने बोलते बहुत कम देखा था पर उनकी आंखें हमेशा पनीली रहती थीं। मुझे याद है मैंने अपने पापा से पूछा था कि अप्पुपन याने दादाजी की आंखें ऐसी क्यों हैं? पापा चुप रह गए थे लेकिन मैं बाद में समझ पाई कि जिस बाप का बेटा कई हज़ार किलोमीटर दूर जाकर बस गया हो, उसकी आंखें और मन हमेशा भीगे ही रहते हैं। हम जीतने दिन वहाँ रहते दादाजी हमारे आस-पास बने रहते। रुंधी आवाज़ में कभी दो शब्द बोले तो बोले वरना वही खामोशी। शायद जितनी हिचक मुझे मलयालम न बोल पाने की हो शायद उतनी ही दादाजी को हिन्दी न समझ पाने की रही हो।
मैंने ददिहाल को हमेशा अपने पिता की नज़र से देखा। वहां मैं, पापा और दादाजी घर के आसपास फ़ैली कई एकड़ ज़मीन पर दिन भर घूमते रहते। मैं लड़खड़ाती तो दादाजी की रूखी हथेली मेरी कलाई थाम लेते… वो स्पर्श मुझे अब भी याद है। मुझे याद है वहां जाकर अपने पिता का बच्चा बन जाना। जब दादाजी उन्हें ‘कुट्टन’ कह कर पुकारते, तो उनकी आंखों के कोर गीले हो जाते और मेरी आंखें चमक जाती थी जब अप्पुपन(मेरे दादा) मुझे कुट्ट-कुट्टी बुलाते… याने बेटे की बेटी।
मेरा गाँव मुझे शरारतें नहीं याद दिलाता है, मेरा गाँव मुझे अपनों से दूर चले जाने की टीस का एहसास कराता है। मैंने ये टीस, ये तकलीफ़ अपने दादा और अपने पिता की आंखों में एक साथ देखी थी।
हमारे घर के ठीक सामने एक छोटी सी प्रतिमा थी किसी छोटे कद के आदिवासी आदमी की। दादाजी बताया करते थे कि ये एक बहादुर था, जिसने आदमखोर शेर को मार कर गाँव वालों को बचाया था। इसलिए उन्होंने उसकी मूर्ती बनवाई। ये बात इसलिए बड़ी थी कि उस दौर में केरल में जातिवाद बहुत ज़ोर पर था और इस वीर का कुल ऊंचा नहीं माना जाता था। उस वक्त उसकी प्रतिमा बनवाकर उसे महिमामंडित करना समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था पर आज उस प्रतिमा पर श्रद्धालु फूल चढ़ा कर माथा टेकते हैं। तब मंदिर को लेकर मुझे दादाजी की खुली सोच और सामाजिक बदलाव जैसी बड़ी बात नहीं समझ आई होगी शायद। तब मेरे लिए वो मंदिर था एक ज़रिया जिसके कारण रोज़ सुबह अलग अलग तरह का प्रसाद मिलता और कुछ चवन्नी अठन्नी भी। थोड़े में खुश होने का वरदान हर बच्चे की तरह मुझे भी तो मिला हुआ था।
आज भी हमारा परिवार उस मंदिर का हिस्सा है। जो मुझे थोड़ा से गर्व से भर देता है।
केरला(Kerala) पूर्ण रूप से साक्षर प्रदेश है यानी वहां का हर बाशिंदा पढ़ा लिखा है और इसलिए वहां लोग बहुत जागरूक हैं। उन दिनों हमारे घर काम करने आने वाली हेल्पर भी फुर्सत पाते ही अखबार खोल कर बैठ जाती थी। मैं सारा दिन उन्हीं के आसपास मंडराती रहती थी, हर लड़की की तरह मुझे भी घर-घर खेलना अच्छा लगता था। वो कभी ओखली में लंबे-लंबे डंडों से नारियल कूटना सिखाती , तो कभी सिल पर मसाले पीसना और सुपारी की छाल से स्पेचुला बनाना, कटहल के पत्तों से टेबल स्पून बनाना भी। घर की रसोई के पास बना कुआं एक ऐसी जगह थी जहां हमारा जाना मना था। मैं मुंडेर पर झुक के ज़रा सा झाँकती तो दूर कहीं से दादाजी की आवाज़ सुनाई देती… उसकी टोका टाकी इसलिए भी ज़्यादा थी क्यूंकि हम शहरी बच्चों के लिए गाँव अनजान था ये वो समझते थे।
घर से ज़रा सी दूर बहती पम्पा नदी के किनारे बैठे मैंने न जाने कितनी कहानियां दादाजी से सुनी होंगी, जिनके पात्र या तो मछुआरे थे या धान की खेती में जुटे मजदूर या मसाले उगाने वाले व्यापारी। मैं अब समझी कि कैसे खेल खेल में वो मुझे अपने गाँव, अपने प्रदेश से जोड़ने की कोशिश करने में लगे थे। दादाजी के देहांत के बाद हम वहां कभी नहीं गए…कोई पुकारने वाला जो नहीं था।
वहाँ से आते हुए पापा अपने साथ घर के बागीचे से एक मुट्ठी मिट्टी उठा लाए थे, जो हमने उनके अंतिम समय में उनके हाथ में रख दी थी। शायद वो ऐसा ही चाहते होंगे। सोचती हूँ तो मन भर भर आता है।
जाउंगी फिर कभी…बिना किसी के पुकारे….अपने लिए अपने गाँव की एक मुट्ठी मिट्टी मुझे भी तो लानी है।